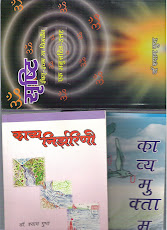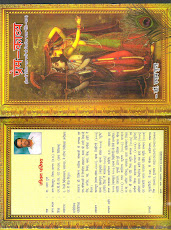---उपरोक्त कवितायेँ पंजाब के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुरजीत सिंह 'पातर' की हैं, जिन्हें हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया है | दोनों कवितायेँ क्या आप की समझ में आती हैं ? सामान्य जन क्या उनका अर्थ समझा पायेगा?
---उपरोक्त कवितायेँ पंजाब के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुरजीत सिंह 'पातर' की हैं, जिन्हें हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया है | दोनों कवितायेँ क्या आप की समझ में आती हैं ? सामान्य जन क्या उनका अर्थ समझा पायेगा?--पहले आदिका को लें ---यह मेरे रक्त के लिपि के उदास अक्षर......(यह= ये होना चाहिए क्योंकि कवि सब कुछ बहुबचन में प्रयोग कररहा है --हो सकता है यह पंजाबी से हिन्दी अनुवादक महोदय के हिन्दी ज्ञान का उदाहरण हो )...क्या सामान्य व्यक्ति ( वास्तव में जिसे समझाने के आवश्यकता है ) इस कठिन कविता के अर्थ को समझ पायेगा ? अब विद्वान् साहित्यकार सोचेंगे व कहेंगे कि--रक्त की लिपि ...=कवि या जनता के परेशान मन से उठे सवाल, लेख आदि; अँधेरे के शब्द= मन व समाज में फैले अन्धकार के आवाज़; उदास उपनिषद् = शास्त्रीय मर्यादाओं का हनन .......आदि-आदि |
----बूढ़ी जादूगरनी को लें --क्या आप कुछ समझ पाए, क्या जन सामान्य इसके गूढार्थ समझ पायेगा | अब शास्त्रकार , साहित्याचार्य --कह सकते हैं कि यह बूढ़ी जादूगरनी- अमर्यादा, अनैतिकता, आतंकवाद, या कुत्सित राज़नीति , या फिर किस्मत आदि आदि हो सकती है , जो पुनः पुनः नए-नए रूप धरकर आती रहती है , चिर युवा --क्या सामान्य जन समझा पायेगा ? या उसके पास इतना समय, धैर्य,ज्ञान है ?-------साहित्य में इसी प्रकार के विद्वता प्रदर्शन , दूरस्थ भाव प्रचलन से साहित्य जन सामान्य से दूर होता जारहा है | सूर-तुलसी-कबीर-मीरा-आदि के शाश्वत -चिर जीवी शब्दों में कौन से दूरस्थ भाव हैं , तभी वह जन-जन के निकट है व समाज व मानव को आज तक दिशा प्रदान कर रहे हैं |कविता अभिधात्मक भाषा में जन सामान्य के निकट होगी तभी वह जनता के समीप पहुंचेगी और जन उसके समीप |