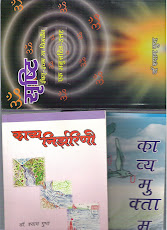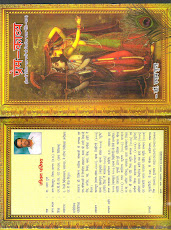....कर्म की बाती,ज्ञान का घृत हो,प्रीति के दीप जलाओ...
रोशनी आँख की बह जायेगी आसूं बन कर
रो रहा था कि तेरे साथ हँसा था बरसों
हँस रहा हूँ कि कोई देख न ले दीदा ए-तर
भारत में शायरी व गज़ल फारसी के साथ सूफी-संतों के प्रभाववश प्रचलित हुई जिसके छंद संस्कृत छंदों के समनुरूप होते हैं | फारसी में गज़ल के विषय रूप में सूफी प्रभाव से शब्द इश्के-मजाज़ी के होते हुए भी अर्थ रूप में ‘इश्के हकीकी’ अर्थात ईश्वर-प्रेम, भक्ति, अध्यात्म, दर्शन आदि सम्मिलित होगये | प्रेमी को साधक और प्रेमिका को ब्रह्म का दर्जा मिल गया। सूफी साधना विरह प्रधान साधना है। इसलिए फ़ारसी ग़ज़लों में भी संयोग के बजाय वियोग पक्ष को ही प्रधानता मिली।
फारसी से भारत में उर्दू में आने पर सामयिक राजभाषा के कारण विविध सामयिक विषय व भारतीय प्रतीक व कथ्य आने लगे
| प्रारंभिक दौर में उर्दू गज़ल में श्रंगार के दोनों पक्षों संयोग-वियोग का ही वर्णन रहता था लेकिन बाद में उसमें परिवर्तन आया। उसमें उपदेश, नीति, चिंतन और देश-प्रेम की बातों का ज़िक्र किया जाने लगा यथा---
जब मैंने विभिन्न शायरों की शायरी—गज़लें व नज्में आदि सुनी-पढीं व देखीं विशेषतया गज़ल...जो विविध प्रकार की थीं..बिना काफिया, बिना रदीफ, वज्न आदि का उठना गिरना आदि ...तो मुझे ख्याल आया कि बहरों-नियमों आदि के पीछे भागना व्यर्थ है, बस लय व गति से गाते चलिए, गुनगुनाते चलिए गज़ल बनती चली जायगी, जो कभी मुरद्दस गज़ल होगी या मुसल्सल या हम रदीफ, कभी मुकद्दस गज़ल होगी या कभी मुकफ्फा गज़ल, कुछ फिसलती गज़लें होंगी कुछ भटकती ग़ज़ल| हाँ लय गति यति युक्त गेयता व भाव-सम्प्रेषणयुक्तता
तथा सामाजिक-सरोकार युक्त
होना चाहिए और आपके पास भाषा, भाव, विषय-ज्ञान व कथ्य-शक्ति होना चाहिए| यह बात गणबद्ध छंदों के लिए भी सच है | तो कुछ शे’र आदि जेहन में यूं चले आये.....
.
बात शायरी की- अंदाज़े बयाँ श्याम का
शायरी अरबी, फारसी व उर्दू जुबान की काव्य-कला है | इसमें गज़ल, नज़्म, रुबाई, कते व शे’र आदि विविध छंद व काव्य-विधाएं प्रयोग होती हैं, जिनमें गज़ल सर्वाधिक लोकप्रिय हुई | गज़ल व नज़्म में यही अंतर है कि नज़्म एक काव्य-विषय व कथ्य पर आधारित काव्य-रचना है जो कितनी भी लंबी, छोटी व अगीत की भांति लघु होसकती है एवं तुकांत या अतुकांत भी | गज़ल मूलतः शे’रों (अशार या अशआर) की मालिका होती है और प्रायः इसका प्रत्येक शे’र विषय–भाव में स्वतंत्र होता है |
नज़्म विषयानुसार तीन तरह की होती हैं ---मसनवी अर्थात प्रेम अध्यात्म, दर्शन व अन्य जीवन के विषय, मर्सिया ..जिसमें दुःख, शोक, गम का वर्णन होता है और कसीदा यानी प्रशंसा जिसमें व्यक्ति विशेष का बढ़ा-चढा कर वर्णन किया जाता है | एक लघु अतुकांत नज्म पेश है...
सच,
यह तुलसी कैसी शांत है
और कश्मीर की झीलें
किस-किस तरह
उथल-पुथल होजाती हैं
और अल्लाह
मैं ! ...........मीना कुमारी
...
रुबाई मूलतः अरबी फारसी का स्वतंत्र ..मुक्तक है जो चार पंक्तियों का होता है इनमें एक ही विषय व ख्याल होता है और कथ्य चौथे मिसरे में ही मुकम्मिल व स्पष्ट होता है | तीसरे मिसरे के अलावा बाकी तीनों मिसरों में काफिया व रदीफ एक ही तुकांत में होते हैं तीसरा मिसरा इस बंदिश से आज़ाद होता है | परन्तु रुबाई में पहला –तीसरा व दूसरा –चौथा मिसरे के तुकांत भी सम होसकते हैं और चारों के भी | फारसी शायर ...उमर खय्याम की रुबाइयां विश्व-प्रसिद्द हैं |..उदाहरण- एक रुबाई....
“ इक नई नज़्म कह रहा हूँ मैं
अपने ज़ज्वात की हसीं तहरीर |
किस मौहब्बत से तक रही है मुझे,
दूर रक्खी हुई तेरी तस्वीर || “ .... निसार अख्तर
कतआ भी हिन्दी के मुक्तक की भांति चार मिसरों का होता है, यह दो शे’रों से मिलकर बनता है | इसमें एक मुकम्मिल शे’र होता है..मतला तथा एक अन्य शे’र होता है| जब शायर ..एक शेर में अपना पूरा ख्याल ज़ाहिर न कर पाए तो वो उस ख्याल को दुसरे शेर से मुकम्मल करता है । कतआ शायद उर्दू में अरबी-फारसी रुबाई का विकसित रूप है| अर्थात दो शे’रों की गज़ल| एक उदाहरण पेश है....
दिल को जो जी पाये |
जख्मे-दिल को जो सी पाए |
दर्दे-ज़मां ही ख्वाव है जिसका
खुदा भी उस दिल में ही समाये ||”... डा श्याम गुप्त
शे’र दो पंक्तियों की शायरी के नियमों में बंधी हुई वह रचना है जिसमें पूरा भाव या विचार व्यक्त कर दिया गया हो | 'शेर' का शाब्दिक अर्थ है --'जानना' अथवा किसी तथ्य से अवगत होना और शायर का अर्थ जानने वाला ...अर्थात ‘कविर्मनीषी स्वयंभू परिभू ...क्रान्तिदर्शी ...कवि
| इन दो पंक्तियों में शायर या कवि अपने पूरे भाव व्यक्त कर देता है ये अपने आप में पूर्ण होने चाहिए उन पंक्तियों के भाव-अर्थ समझाने के लिए किन्हीं अन्य पंक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए | गज़ल शे’रों की मालिका ही होती है | अपनी सुन्दर तुकांत लय, गति व प्रवाह तथा प्रत्येक शे’र स्वतंत्र व मुक्त विषय-भाव होने के कारण के कारण साथ ही साथ प्रेम, दर्द, साकी–ओ-मीना कथ्यों व वर्ण्य विषयों के कारण गज़ल विश्वभर के काव्य में प्रसिद्द हुई व जन-जन में लोकप्रिय हुई | ऐसा स्वतंत्र शे’र जो तन्हा हो यानी किसी नज़्म या ग़ज़ल या कसीदे या मसनवी का पार्ट न हो ..उसे फर्द कहते हैं |
गज़ल दर्दे-दिल की बात बयाँ करने का सबसे माकूल व खुशनुमां अंदाज़ है | इसका शिल्प भी अनूठा है | नज़्म व रुबाइयों से जुदा | इसीलिये विश्व भर में जन-सामान्य में प्रचलित हुई | हिन्दी काव्य-कला में इस प्रकार के शिल्प की विधा नहीं मिलती | मैं कोई शायरी व गज़ल का विशेषज्ञ ज्ञाता नहीं हूँ | परन्तु हम लोग हिन्दी फिल्मों के गीत सुनते हुए बड़े हुए हैं जिनमें वाद्य-इंस्ट्रूमेंटेशन की सुविधा हेतु गज़ल व नज़्म को भी गीत की भांति प्रस्तुत किया जाता रहा है |
....यथा…. साहिर लुधियानवी की प्रसिद्द हिन्दी ग़ज़ल...
संसार
से भागे फिरते
हो संसार को तुम
क्या पाओगे।
इस लोक
को भी अपना
न सके उस लोक
में भी पछताओगे।
हम कहते
हैं ये जग अपना
है तुम कहते
हो झूठा सपना
है
हम जन्म
बिता कर जाएंगे
तुम जन्म गँवाकर
जाओगे।
छंदों व गीतों के साथ-साथ दोहा व अगीत-छंद लिखते हुए व गज़ल सुनते, पढते हुए मैंने यह अनुभव किया कि उर्दू शे’र भी संक्षिप्तता व सटीक भाव-सम्प्रेषण में दोहे व अगीत की भांति ही है और इसका शिल्प दोहे की भांति ...अतः लिखा जा सकता है, और नज्में तो तुकांत-अतुकांत गीत के भांति ही हैं, और गज़लों–नज्मों का सिलसिला चलने लगा |
गज़ल मूलतः अरबी भाषा का गीति-काव्य है जो काव्यात्मक अन्त्यानुप्रास युक्त छंद है और अरबी भाषा में “कसीदा” अर्थात प्रशस्ति-गान हेतु प्रयोग होता था जो राजा-महाराजाओं के लिए गाये जाते थे एवं असहनीय लंबे-लंबे वर्णन युक्त होते थे जिनमें औरतों व औरतों के बारे में गुफ्तगू एक मूल विषय-भाग भी होता था | कसीदा के उसी भाग “ताशिब “ को पृथक करके गज़ल का रूप व नाम दिया गया |
गज़ल शब्द अरबी रेगिस्तान में पाए जाने वाले एक छोटे, चंचल पशु हिरण ( या हिरणी, मृग-मृगी ) से लिया गया है जिसे अरबी में ‘ग़ज़ल’ (ghazal या
guzal ) कहा जाता है | इसकी चमकदार, भोली-भाली नशीली आँखें, पतली लंबी टांगें, इधर-उधर उछल-उछल कर एक जगह न टिकने वाली, नखरीली चाल के कारण उसकी तुलना अतिशय सौंदर्य के परकीया प्रतिमान वाली स्त्री से की जाती थी जैसे हिन्दी में मृगनयनी | अरबी लोग इसका शिकार बड़े शौक से करते थे | अतः अरब-कला व प्रेम-काव्य में स्त्री-सौंदर्य, प्रेम, छलना, विरह-वियोग, दर्द का प्रतिमान ‘गज़ल’ के नाम से प्रचलित हुआ| जैसे भारतीय काव्य-गीतों में वीणा–सारंग का पीड़ात्मक-भावुक प्रसंग |
शायर फिराक गोरखपुरी के अनुसार जब कोई शिकारी जंगल में कुत्तों के साथ हिरन का पीछा करता हैं और हिरन भागते-भागते झाड़ी में फंस जाता है और निकल नहीं पाता, उस समय उसके कंठ से एक दर्द भरी आवाज निकलती है, उसी करूण स्वर को गजल कहते हैं. इसलिये विवशता का दिव्यतम रूप में प्रकट होना, स्वर का करूणतम हो जाना ही गजल का आदर्श है |
यही गज़ल का अर्थ भी ..अर्थात ‘इश्के-मजाज़ी‘ - आशिक-माशूक वार्ता या प्रेम-गीत, जिनमें मूलतः विरह-वियोग की उच्चतर अभिव्यक्ति होती है |इसीलिये ग़ज़ल में शमा-परवाना, दीपक-शलभ, गुल-बुलबुल, कलिका-भ्रमर आदि प्रसंग प्रभावी हुए | गज़ल ईरान होती हुई सारे विश्व में फ़ैली और जर्मन व इंग्लिश में काफी लोक-प्रिय हुई | यथा..
अमेरिकी अंग्रेज़ी शायर ..आगा शाहिद अली कश्मीरी की एक अंग्रेज़ी गज़ल का नमूना पेश है...
Where are you
now? who lies beneath your spell
tonight ?
Whom
else rapture’s road
will you expel
to night ?
My
rivals for your love,
you have invited
them all .
This is
mere insult , this
is no farewell
to night .
गज़ल का मूल छंद शे’र या शेअर है | शेर वास्तव में ‘दोहा’ का ही विकसित रूप है जो संक्षिप्तता में तीब्र व सटीक भाव-सम्प्रेषण हेतु सर्वश्रेष्ठ छंद है | आजकल उसके अतुकांत रूप-भाव छंद ..अगीत, नव-अगीत व त्रिपदा-अगीत भी प्रचलित हैं| अरबी, तुर्की फारसी में भी इसे ‘दोहा’ ही कहा जाता है व अंग्रेज़ी में कसीदा मोनो राइम( quasida
mono rhyme)| अतः जो दोहा में सिद्धहस्त है अगीत लिख सकता है वह शे’र भी लिख सकता है..गज़ल भी | शे’रों की मालिका ही गज़ल है |ग़ज़लों के ऐसे संग्रह को जिसमें हर हर्फ से कम से कम एक ग़ज़ल अवश्य हो दीवान कहते हैं।
तुकांतता के अनुसार ग़ज़लें मुअद्दस या
मुकफ्फा होती है| मुअद्दस
गज़ल में रदीफ और काफिया दोनों का ध्यान रखा जाता है इसे मुरद्दफ़
ग़ज़ल भी कहते हैं .. यथा ....
उनसे
मिले
तो
मीना
ओ
सागर
लिए
हुए,
हमसे मिले तो जंग का तेवर लिए हुए
लड़की किसी ग़रीब की सड़कों पे आ गई
गाली लबों पे हाथ में पत्थर लिए हुए |... - (जमील हापुडी)
एवं मुकफ्फा ग़ज़ल में केवल काफिया का ध्यान रखा जाता है इसे ग़ैर मुरद्दफ़ या गैर रदीफ़ ग़ज़ल भी कहते हैं| जैसे...
जाने वाले तुझे कब देख सकूं बारे दीगरहमसे मिले तो जंग का तेवर लिए हुए
लड़की किसी ग़रीब की सड़कों पे आ गई
गाली लबों पे हाथ में पत्थर लिए हुए |... - (जमील हापुडी)
एवं मुकफ्फा ग़ज़ल में केवल काफिया का ध्यान रखा जाता है इसे ग़ैर मुरद्दफ़ या गैर रदीफ़ ग़ज़ल भी कहते हैं| जैसे...
रोशनी आँख की बह जायेगी आसूं बन कर
रो रहा था कि तेरे साथ हँसा था बरसों
हँस रहा हूँ कि कोई देख न ले दीदा ए-तर
ग़ज़ल में ग़ज़ल
का
प्रत्येक शे'र अपने आप में पूर्ण होता है तथा शायर ग़ज़ल के प्रत्येक शे'र में अलग अलग भाव को व्यक्त कर सकता है | जब किसी ग़ज़ल के सभी शेर एक ही भाव को केन्द्र मान कर लिखे गए
हों
तो
ऐसी
ग़ज़ल
को
मुसल्सल ग़ज़ल कहते हैं| यदि ग़ज़ल के प्रत्येक शे'र अलग अलग भाव को व्यक्त करें तो ऐसी ग़ज़ल को ग़ैर
मुसल्सल ग़ज़ल कहते हैं
वस्तुतः काव्य के मूल भाव के अनुरूप ग़ज़ल में भी तकनीक की अपेक्षा भाव, प्रभावोत्पादकता व प्रवाह ही अच्छी ग़ज़ल की पहचान है जिसमें मौलिकता हो, जिससे गीत व कविता की ही भांति पढ़ने वाला समझे कि यह उस की स्वयं की दिल की बातों का वर्णन है | प्रायः सुरूचिपूर्ण व जाने-पहचाने और सरल शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए | क्लिष्ट शब्द प्रवाह, गति, सम्प्रेषणता एवं काव्यानंद में अवरोध उत्पन्न करते हैं |भाव चाहे कितना भी उच्च हो, छंद चाहे कितना ही उपयुक्त व सुंदर हो लेकिन कथ्य की अस्पष्टता व तथ्य की अवास्तविकता एवं उचित शब्द चयन व भाषा व्याकरणीय शब्द क्रम आदि के न होने से ग़ज़ल या कविता प्रभावहीन हो जाती है। अस्पष्ट भाव, कथ्य एवं तथ्य के बारे में एक प्रसिद्द शेर है-
मगस कोयूं बाग
में
जाने
न
दीजिये
महज़
परवाने
बर्बाद
होजाएंगे |
शेर सुन्दर है लेकिन उसका
अर्थ समझ के परे है।
व्याख्या
है कि - ऐ माली तू मगस (मधुमक्खी) को बाग में न जाने दे| वह गुलों का रस चूस कर पेड़ पर शहद का छत्ता
बनायेगी ,उस से मोम निकलेगा, उससे शमा बनेगी | जब शमा जलेगी तो बेचारा परवाना उस पर मंडराएगा और बिना वजह जल कर राख हो जाएगा।
शब्द क्रम आदि व्याकरण भाव भी हिन्दी में अत्यंत महत्त्व रखता है |( विश्व में केवल एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें शब्द-क्रम कुछ भी हो अर्थ वही रहता है ) ग़ज़ल में उर्दू शब्दों के प्रयोग से शब्द क्रम का ख्याल न रहने से अर्थ-अनर्थ होजाता है देखिये ...
कहाँ
खो गई उसकी
चीखें हवा में
हुआ
जो परिंदा ज़िबह
ढूँढता है-
कवि कहना चाहता है कि कत्ल (जिबह ) हुआ पंछी हवा में खो गई अपनी 'चीखें' ढूँढ रहा है। लेकिन 'ज़िबह' शब्द गलत जगह पर आने से अर्थ यही निकलता है कि वह ज़िबह की तलाश में है।
सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं
देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में हैं
वक्त आने दे बताएंगे तुझे ऐ आसमाँ
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। - --राम प्रसाद बिस्मिल
उर्दू से हिन्दुस्तानी व हिन्दी में आने पर गज़ल में वर्ण्य-विषयों का एक विराट संसार निर्मित हुआ और हर भारतीय भाषा में गज़ल कही जाने लगी | तदपि साकी, मीना ओ सागर व इश्के-मजाज़ी गजल का सदैव ही प्रिय विषय बना रहा | बकौल मिर्जा गालिव....
“बनती नहीं है वादा ओ सागर कहे बगैर “ |
यूं तो हिन्दी में ग़ज़ल कबीरदास जी द्वारा भी कही गयी बताई जाती है जिसे कतिपय विद्वानों द्वारा हिन्दी की सर्वप्रथम ग़ज़ल कहा जाता है, यथा....
“ हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या ?
रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या ?
कबीरा इश्क का मारा, दुई को दूर कर दिल से,
जो चलना राह नाज़ुक है, हमन सर बोझ भारी क्या ? “
परन्तु मेरे विचार से इस ग़ज़ल की भाषा कबीर की भाषा से मेल नहीं खाती | हो सकता है यह प्रक्षिप्त हो एवं कबीर नाम के किसी और गज़लकार ने इसे कहा हो|
वास्तव में तो हिन्दी में गज़ल का प्राम्म्भ आगरा में जन्मे व पले शायर ‘अमीर खुसरो’ (१२-१३ वीं शताब्दी) से हुआ जिसने सबसे पहले इस भाषा को ‘हिन्दवी’ कहा और वही आगे चलकर ‘हिन्दी’ कहलाई | खुसरो अपने ग़ज़लों के मिसरे का पहला भाग फारसी या उर्दू में व दूसरा भाग हिन्दवी में कहते थे | उदाहरणार्थ...
“ जेहाले मिस्कीं मकुल तगाफुल,
दुराये नैना बनाए बतियाँ |
कि ताब-ए-हिजां, न दारम-ए-जाँ, 4.
न लेहु काहे लगाय छतियाँ |”
१७ वीं सदी में उर्दू के पहले शायर ‘वली’ ने भी हिन्दी को अपनाया व देवनागरी लिपि का प्रयोग किया | ..यथा....
“सजन सुख सेती खोलो नकाब आहिस्ता-आहिस्ता,
कि ज्यों गुल से निकलता है गुलाव आहिस्ता-आहिस्ता |
सदियों तक गज़ल राजा-नबावों के दरबारों में सिर्फ इश्किया मानसिक विचार बनी रही जिसे उच्च कोटि की कला माना जाता रहा | परन्तु १८ वीं सदी में आगरा के नजीर अकबरावादी ने शायरी को सामान्य जन से जोड़ा और १९ वीं सदी के प्रारम्भ में मिर्ज़ा गालिव ने मानवीय जीवन के गीतों से | उदाहरणार्थ.....
”जब फागुन रंग झलकते हों, तब देख बहारें होली की |
परियों के रंग दमकते हों, तब देख बहारें होली की |” -
....... नजीर अकबरावादी तथा....
“गालिव बुरा न मान जो वाइज़ बुरा कहे ,
ऐसा भी है कोई कि सब अच्छा कहें जिसे |
-------गालिव ...
१८ वीं सदी में हिन्दी में गज़ल की पहल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद आदि ने सरोकारों की अभिव्यक्ति व लोक-चेतना के स्वर दिए..यथा निराला ने कहा...
“लोक में बंट जाय जो पूंजी तुम्हारे दिल में है “
त्रिलोचन, शमशेर, बलबीर सिंह ‘रंग’ ने भी हिन्दी ग़ज़लों को आयाम दिए | परन्तु आधुनिक खड़ी बोली में हिन्दी-गज़ल के प्रारम्भ का श्रेय दुष्यंत कुमार को दिया जाता है जिन्होंने हिन्दी भाषा में गज़लें लिख कर गज़ल के विषय भावों को राजनैतिक, संवेदना, व्यवस्था, सामाजिक चेतना आदि के नए नए आयाम दिए | वस्तुतः हिन्दी भाषा ने अपने उदारचेता स्वभाववश उर्दू-फारसी के तमाम
शब्दों को भी अपने में समाहित किया,
अतः आज के अद्यतन समय में हिन्दी कवियों
ने भी ग़ज़ल को अपनाया है व समृद्ध किया है फलस्वरूप आज गज़ल व हिन्दी -गज़ल में
विषयों व
ग़ज़लकारों का एक विराट रचना संसार है जो प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, रचनाओं एवं अंतर्जाल( इंटरनेट) पर प्रकाशन
द्वारा समस्त विश्व में फैला हुआ है तथा जो उर्दू गज़ल, हिन्दी ग़ज़ल, शुद्ध खड़ी-बोली, हिन्दी एवं हिन्दी की सह-बोलियों के शुद्ध व मिश्रित रूपों से समस्त
शायरी-विधा व ग़ज़ल को समर्थ वसमृद्ध कर रहे
है | ... दुष्यंत कुमार की एक गज़ल देखिये....
“दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है,
आजकल नेपथ्य में संभावना है |”
वस्तुतः हिन्दी भाषा ने अपने उदारचेता स्वभाववश उर्दू-फारसी के तमाम शब्दों को भी अपने में समाहित किया, अतः आज के अद्यतन समय में हिन्दी कवियों ने भी ग़ज़ल को अपनाया व समृद्ध किया है| हिन्दी गजल के पास अपनी विराट शब्द-संपदा है, मिथक हैं, मुहावरे, बिम्ब, प्रतीक, व रदीफ - काफिये हैं। आज हिन्दी- गजल में पारम्परिक गजल की काव्य-रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास है तथा नए शिल्प और विषय का उत्तरोत्तर विकास का भी| फलस्वरूप आज गज़ल व हिन्दी -गज़ल में विषयों व ग़ज़लकारों का एक विराट रचना संसार है जो प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, रचनाओं एवं अंतर्जाल( इंटरनेट) पर प्रकाशन द्वारा समस्त विश्व में फैला हुआ है तथा जो उर्दू गज़ल, हिन्दी ग़ज़ल, शुद्ध खड़ी-बोली, हिन्दी एवं हिन्दी की सह-बोलियों के शुद्ध व मिश्रित रूपों से समस्त शायरी-विधा व ग़ज़ल को समर्थ व समृद्ध कर रहे है तथा दिन ब दिन ग़ज़ल में गीतिका, नई ग़ज़ल आदि नाम से नए-नए प्रयोग भी होरहे हैं|
मेरे विचार से हिन्दी ग़ज़ल के लिए एक जरूरी बात यह है कि हिन्दी व्याकरण की परिधि में शब्दों का विभाजन हो और मात्रा की गणना भी, ताकि ग़ज़ल
के शिल्प और कथ्य में तारतम्य रह सके | उर्दू ज़बान का हिन्दी गज़ल पर हावी होना उसके स्वरूप के निखार में बाधक है। हिन्दी की अनेक गज़लें तो लगती हैं जैसे वे उर्दू की हैं उनमें हिन्दी की वह अपनी सोंधी-सोंधी सुगंध है ही नहीं एवं वह अरबी-फारसी के लफ्जों से दब कर रह गई है। हिन्दी की एक ग़ज़ल
का हिस्सा देखिये...
साहित्य सत्यं शिवं सुन्दर भाव होना चाहिए ,
साहित्य शुचि शुभ ज्ञान पारावार होना चाहिए |
ललित भाषा ललित कथ्य न सत्य तथ्य परे रहे ,
व्याकरण शुचि सुद्ध सौख्य समर्थ होना चाहिए |.. ...डा श्याम गुप्त
यदि हिन्दुस्तानी भाषा के अनुरूप हिन्दी में घुलमिल गए उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो जो
सहज ही आजायें तो सौन्दर्य, प्रभाव व सम्प्रेषण
की स्पष्टता बढ़ सकती है | यथा एक ग़ज़ल देखें .
वो हारते हे कब हें जो सजदे में झुक लिए
यूं फख्र से जियो यूंही चलती रहे ये ज़िंदगी | ---डा श्याम गुप्त
चूँकि गज़ल मूलतःउर्दू से से हिन्दी में आई है इसलिए यह मान लेना कि जब तक उसमें उर्दू के कुछ लफ्ज़ अवश्य हों उचित नहीं। अतः मेरे विचार में फ़ारसी, और उर्दू के क्लिष्ट शब्दों से परहेज़ करना ही उचित है | उदाहरणार्थ ऐसे उर्दू /फारसी शब्दों
के प्रयोग का क्या लाभ जिसे हिन्दी वाले तो क्या उर्दू भाषी भी न समझ पायें...उदाहरणार्थ
तहज़ीबो तमद्दुन
है
फ़कत नाम के लिए
गुम हो गई शाइस्तगी
दुनिया की भीड़ में ---- कुँवर कुसुमेश
होना चाहिए और आपके पास भाषा, भाव, विषय-ज्ञान व कथ्य-शक्ति होना चाहिए| यह बात गणबद्ध छंदों के लिए भी सच है | तो कुछ शे’र आदि जेहन में यूं चले आये.....
“मतला बगैर हो गज़ल, हो रदीफ भी नहीं,
यह तो गज़ल नहीं, ये कोइ वाकया नहीं |
लय गति हो ताल सुर सुगम, आनंद रस बहे,
वह भी गज़ल है, चाहे कोई काफिया नहीं | “
------डा श्याम गुप्त